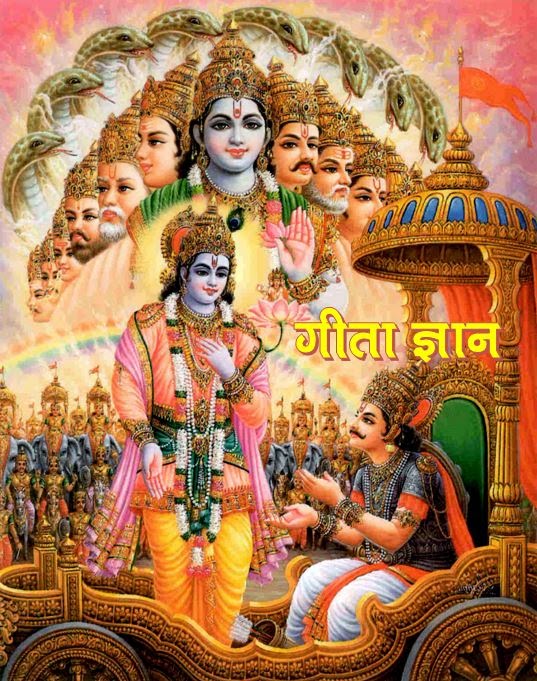अथाष्टादशोऽध्यायः
(मोक्षसंन्यास योग)
(भाग-1)
(भाग-1)
यह अध्याय गीता का अंतिम अध्याय है, अतः उपसंहारात्मक है। उपसंहार में पूर्व कथ्यों पर विहंगम दृष्टि, रचनाकार के मत की स्थापना अथवा निष्कर्ष होता है। इसी कारण से यह गीता का सबसे बड़ा अध्याय है। इसका नामकरण ‘‘मोक्षसंन्यास योग’’ किया गया है, क्योंकि इसमें मोक्ष का भी संन्यास अर्थात् त्याग हो जाता है। इस अध्याय का समापन प्रपत्तिवाद के साथ होता है। प्रपत्ति का अर्थ पूर्ण शरणागति है। इसमें भक्त भगवान् पर पूर्णरूपेण आश्रित होकर चिन्ता-निर्मुक्त हो जाता है। अध्याय बड़ा होने के कारण इसे कुछ भागों में इस ब्लॉग पर प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि पाठक को आसानी हो सके।
इस अध्याय में त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्त्ता, बुद्धि, धृति, सुख, वर्ण-व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के लक्षण, कर्म की महत्ता, परब्रह्म-प्राप्ति का सहज साधन, गीता के पठन एवं श्रवण का माहात्म्य आदि के बारे में कथन उपलब्ध है। अतः इस अध्याय को गीता-सार के रूप में समझने में भी कोई हानि नहीं होगी। चूँकि यह सार-संक्षेप है, अतः इसकी व्याख्या विस्तार से की जायेगी।
इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने संन्यास एवं त्याग के तत्त्व को जानने का आग्रह किया, तो भगवान् कहते हैं कि कुछ विद्वान् काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कुछ विद्वान् सम्पूर्ण कर्मों के फल-त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान् कहते हैं कि कर्मों को दोष की भाँति त्याग देना चाहिए, जबकि कई विद्वान् कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि त्याग से सम्बन्धित चार सिद्धान्त हैंः-
1) काम्य कर्मों का त्याग - अर्थात् इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट की निवृत्ति के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनका त्याग संन्यास है।
2) फल की कामना का त्याग अर्थात् फल की इच्छा न कर कर्मों को करते रहना ही त्याग है।
3) कर्म मात्र का त्याग अर्थात् कर्म को ही दोष के समान जानकर उनका त्याग करना चाहिए।
4) यज्ञ, दान, तप आदि का त्याग न करना अर्थात् इनके अलावा अन्य कर्मों के त्याग करना।
इस विषय में मनुष्य को यह तथ्य जानना बहुत आवश्यक है कि यज्ञ, दान और तपरूपी कर्मों के त्याग नहीं करने चाहिए। ये तो पवित्र करने वाले होते हैं। इनमें जो आसक्ति है और फल की कामना है, उसका त्याग करना चाहिए। नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं है। त्याग सात्त्विक, राजस और तामस तीन श्रेणियों का होता है। नियत कर्मों का मूढ़ता के कारणवश त्याग करना तामस त्याग कहा गया है, क्योंकि नियत कर्मों से छुटकारा संभव नहीं है और यह उचित भी नहीं है। यज्ञ, दान आदि कर्म करने में अनेक कष्टों को उठाना पड़ता है। अनेक प्रकार के दुःख सहने पड़ते हैं। किसी कर्म को, कि वह दुःख है, ऐसा समझकर किसी शारीरिक क्लेश के कारण कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस त्याग कहलाता है। ऐसे त्याग से वास्तविक त्याग का फल नहीं मिलता है।
इसके बाद सात्त्विक त्याग के बारे में भगवान् कहते हैं कि जो कर्म शास्त्रसम्मत है, जब उसे कर्तव्य भाव से आसक्ति एवं फल-त्याग करके किया जाता है, तो वह सात्त्विक त्याग कहलाता है। शरीरधारी पुरुष सम्पूर्ण कर्मों का त्याग चाहकर भी नहीं कर सकता है, अतः जो कर्मफलासक्ति का त्याग करता है, वही सच्चा त्यागी है। जो मनुष्य कर्मफल का त्याग नहीं करता है, उसे मृत्यु के बाद भी तीन प्रकार के फल मिलते हैं। ये हैं इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। इष्ट कर्म वे हैं, जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है और जिस परिस्थिति को नहीं चाहता वे अनिष्ट कर्म हैं। साथ ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जिनमें इष्ट एवं अनिष्ट का मिश्रण होता है। ऐसे कर्मों के फल उन सभी को भोगने ही पड़ते हैं, यदि उन्होंने कर्मफल का त्याग नहीं किया है।
कर्म के बारे में समझने के लिये हमें समझना होगा कि पुरुष एवं प्रकृति भिन्न हैं। पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता, जबकि प्रकृति कभी भी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है। ये कर्म तीन प्रकार के होते हैं - क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो वर्तमान में कर्म किये जाते हैं, वे क्रियमण कर्म हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किये गये तथा अन्य मनुष्य जन्मों के किये गये कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। इस संचित कर्मों से जो कर्मफल देने के लिये उन्मुख हो गये हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं।
क्रियमाण कर्म दो प्रकार के होते हैं - शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि-विधान से किये जाते हैं, वे शुभ कर्म कहलाते हैं। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति से प्रेरित शास्त्रनिषिद्ध कर्म अशुभ कर्म कहलाते हैं। इन समस्त क्रियमण कर्म के एक तो फल-अंश बनता है और दूसरा संस्कार-अंश। इस फल-अंश के दो भाग होते हैं - दृष्ट और अदृष्ट। इसमें दृष्ट के भी दो भेद होते हैं - तात्कालिक और कालान्तरिक। जैसे भोजन करने के समय उसका रस आदि दृष्ट कर्म का तात्कालिक फल है, जबकि उसे भोजन के कारण आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना कालान्तरिक फल है। इसी प्रकार अदृष्ट फल-अंश के भी दो प्रकार होते हैं - लौकिक और पारलौकिक। अपने जीवन में ही यज्ञादि कर्मों के द्वारा पुत्र, धन, यश आदि का मिलना लौकिक फल है। जबकि यज्ञादि कर्मों से जब स्वर्गादि की प्राप्ति होती है तो वह पारलौकिक फल है। यहाँ इस बात को समझना होगा कि इस जीवन में धरती पर भोगे गये फल को लौकिक फल कहते हैं। मनुष्य अपने पापकर्मों को यहीं कैद, जुर्माना, अपमान आदि के रूप में भोगने के बाद यह समझने लगता है कि अब उसे कुछ नहीं भोगना है, किन्तु मनुष्य को यह गणना नहीं होती कि उसने पूरा फल होगा है अथवा अधूरा। ईश्वर को इसकी गणना होती है और फिर उसे वे फल भी भोगने ही पड़ते हैं। चाहे यहाँ इस लोक में अथवा परलोक में।
क्रियमाण कर्म के संस्कार-अंश भी दो प्रकार के होते हैं - शुद्ध एवं पवित्र संस्कार तथा अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार बनते हैं वे पवित्र संस्कार कहलाते हैं और शास्त्रनिषिद्ध कर्म करने से जो संस्कार बनते हैं, वे अपवित्र संस्कार कहलाते हैं।
संचित कर्म के भी फल-अंश और संस्कार-अंश दो होते हैं। संचित कर्म के फल-अंश से मनुष्य का प्रारब्ध बनता है और संस्कार-अंश से स्फुरणा होती रहती है। ये स्फुरणायें मनुष्य को प्रदत्त कार्य करने को विवश करती रहती हैं। यह तब तक होती रहती हैं, जब तक कि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति पर ये स्फुरणायें नहीं आती हैं। अतः जीवनमुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र विचार कभी नहीं आते।
प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं, जो संचित कर्म के फल देने के सम्मुख होते हैं। इन प्रारब्ध कर्मों के फल अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में सामने आते हैं, किन्तु इन प्रारब्ध कर्मों के भोगने के लिये मनुष्य की प्रवृत्ति के तीन प्रकार होते हैं - (1) स्वेच्छापूर्वक (2) अनिच्छापूर्वक और (3) परेच्छापूर्वक। इन स्थितियों को उदाहरण से समझा जा सकता है।
एक व्यापारी धन लगाकर व्यापार करता है और उसे लाभ होता है। दूसरा व्यापारी धन लगाकर व्यापार करता है और उसे हानि होती है। तो यहाँ लाभ और हानि प्रारब्ध के कर्मों के फल हैं, जबकि धन लगाना स्वेच्छापूर्वक है।
किसी व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिल गया। उधर एक व्यक्ति घोड़े से गिरकर अपने पाँव तुड़वा बैठा। धन मिलना एवं पाँव का टूटना शुभ-अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, किन्तु धन का मिलना और पाँव का टूटना अनिच्छापूर्वक है।
किसी व्यक्ति ने एक बच्चे को गोद ले लिया, तो उस व्यक्ति का सारा धन उस बालक को मिल गया, जिसे बाद में चोरों ने चुरा लिया। यहाँ बच्चे को धन मिलना और चोरों द्वारा चुरा लेना शुभ-अशुभ कर्मों के फल हैं, किन्तु गोद में जाना अथवा चोरी होना परेच्छापूर्वक है।
यहाँ जो बात समझने वाली है कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता है, बल्कि परिस्थिति होती है। तात्पर्य यह कि प्रारब्ध कर्मों के फल परिस्थिति के रूप में सामने आते हैं। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल भी प्राप्त फल एवं अप्राप्त फल दो प्रकार के होते हैं। जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ रही हैं, वे प्राप्त फल हैं और जो आगे आने वाली हैं, वे अप्राप्त फल हैं। जब तक संचित कर्म रहते हैं, प्रारब्ध की परिस्थितियाँ बनती ही रहती हैं। यहाँ सामान्य मानव-मन में प्रारब्ध और करने वाले कर्म के मध्य शंका उपस्थित होती है। यदि सभी परिस्थितियाँ प्रारब्ध के कर्मफल के अनुसार ही हों, तो नये कर्म का क्या अर्थ? ऐसे में प्रारब्ध और पुरुषार्थ को जानना आवश्यक हो जाता है।
मनुष्य में चाहना चार प्रकार की होती है - धन की, धर्म की, भोग की और मुक्ति की। इन्हें सरल शब्दों अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष की कामना कहा जाता है। इनमें अर्थ और काम में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है, जबकि धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता और प्रारब्ध की गौणता होती है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दो अलग-अलग क्षेत्र हैं और इनमें भिन्नता है। प्रारब्ध निश्चित है, क्योंकि यह संचित कर्म के फल के रूप में प्राप्त होता है। पुरुषार्थ व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म है, जिसका फल उस कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। यह शरीर पुरुषार्थ के लिये मिला है। इसी पुरुषार्थ से धर्मादि कार्यों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मानव-शरीर सुख-दुख भोगने के लिये नहीं है, क्योंकि उसके लिये स्वर्ग-नरक आदि हैं। यह तो कर्मयोनि है, जहाँ उसे कर्म करना है, जिसका लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है, ताकि वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो सके।
===========
विश्वजीत ‘सपन’